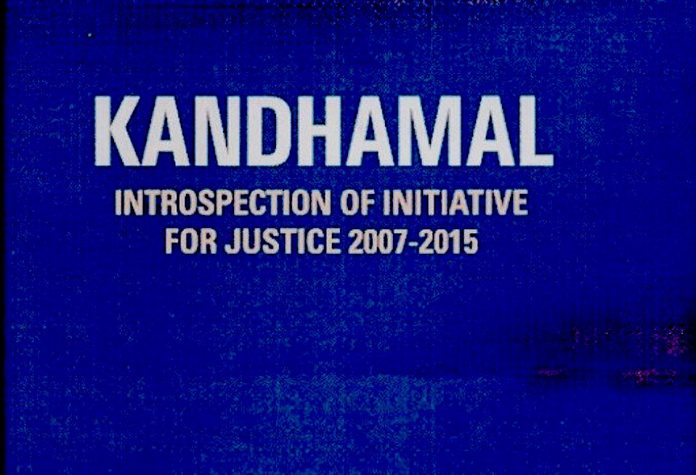विद्या भूषण रावत
ओडिशा के कंधमाल क्षेत्र में दलित और ईसाई आदिवासियों के बीच हुए हिंसा में लगभग सौ से अधिक मौतें हुई. ये हिंसा पहले दिसंबर 2007 में हुई और उसके बाद ज्यादा भयावह तौर पर अगस्त 2008 में हुई. अगस्त 2008 की हिंसा के पीछे स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या को ज़िम्मेवार ठहराया गया, जिसकी हक़ीक़त यह है कि पूरी प्रशासनिक रिपोर्ट ये बताती है कि स्वामी के हत्या के लिए ईसाई मिशनरीज नहीं अपितु नक्सलवादी ज़िम्मेवार हो सकते हैं, लेकिन हिंदुत्ववादी शक्तियों ने ईसाइयों के विरुद्ध अपने ज़हरीले अभियान से पूरे मसले को ईसाई और गैर-ईसाईयो में तब्दील कर दिया.
सरकारी सूचनाओं ने दिसंबर 2008 में मरने वालों की संख्या 39 बताई, जिसमें 2 पुलिस कर्मी और 3 दंगाई भी थे. लेकिन स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले मानवाधिकार संगठनों ने इसकी संख्या सौ से ऊपर बताई है. 600 से अधिक गाँवों को ध्वस्त किया गया और 5600 घरों को लूटा और जलाया गया, जिसमे लगभग 54000 लोग बेघर हो गए. 295 चर्च और अन्य पूजास्थल तोड़ डाले गए. लगभग 30 हज़ार लोग रिलीफ़ कैम्पों में रह रहे हैं और अभी तक विस्थापित ही हैं. 13 स्कूल, कालेज, स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यालय, लेप्रोसी सेंटर आदि भी नष्ट कर दिए गए. लगभग 2000 लोगों को ईसाई धर्म छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया. भय और विस्थापन के चलते 10 हज़ार बच्चे स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो गए.
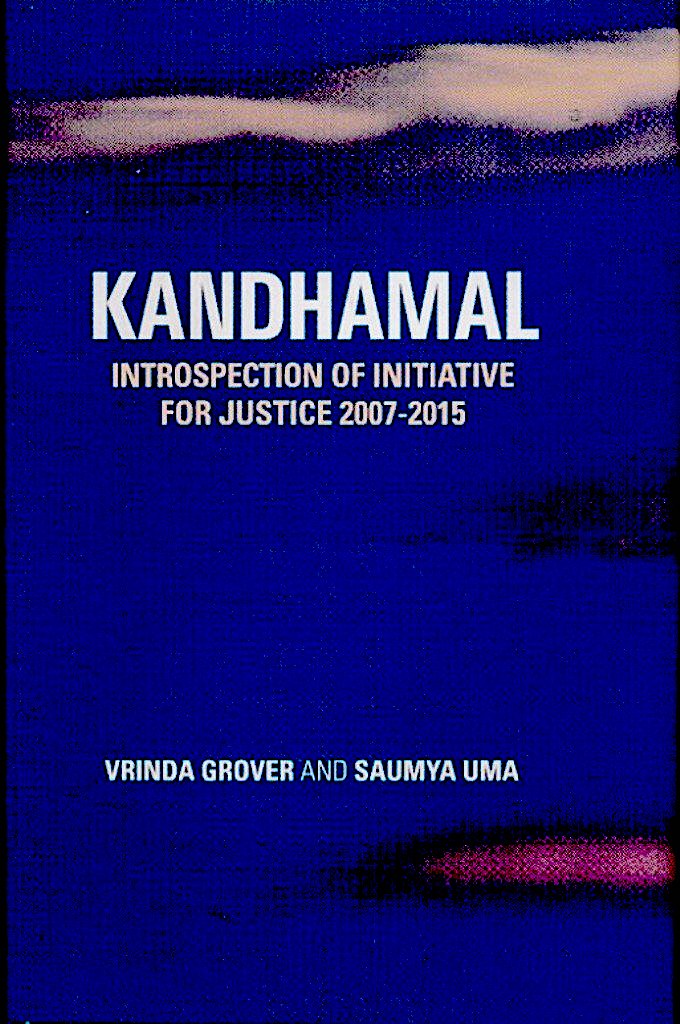
कंधमाल ओडिशा का एक बेहद पिछड़ा हुआ ज़िला है, जहां पर कांध आदिवासियों की बहुतायत है, जिनकी आबादी क्षेत्रीय जनसंख्या का 51 फ़ीसद है, जो क्षेत्र की 77 फ़ीसदी ज़मीन के मालिक हैं. प्रकृति पूजक इन आदिवासियों को ईसाई मिशनरियों और हिन्दू संगठनों ने धर्मांतरण करने के प्रयास किये हैं, जिसके कारण भी यहां पर तनाव बढ़ा.
कंधमाल के ऊपर बने नेशनल पीपल ट्रिब्यूनल में जस्टिस ए.पी. शाह ने कहा, ‘कंधमाल में नरसंहार ईसाई समुदाय, जिसमें बहुसंख्य दलित ईसाई और आदिवासी हैं, और जिन लोगों ने इसका समर्थन किया और समुदाय के साथ काम किया, के विरुद्ध सांप्रदायिक हिंसा है.’
पुस्तक में कंधमाल हिंसा की जाँच के लिए बने जस्टिस पाणिग्रही जांच आयोग और जस्टिस नायडू आयोग की विस्तार पूर्वक समीक्षा की गयी है, जिसमें इन जांच आयोगों की क़ानूनी सीमाओ और भविष्य की रुपरेखा पर भी चर्चा की गयी है.
इस पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भारत के विभिन्न ‘स्वायत्त’ संस्थाओं जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा की गयी जांच के विभिन्न पहलुओं को भी छुआ है, जिसमें राज्य सरकार की आलोचना की गयी है, हालांकि एनएचआरसी की रिपोर्ट के विरोधाभास पर भी टिप्पणी की गयी हैं. स्वायत्त संगठनों की सीमाओं और उनकी रिपोर्ट का इस सन्दर्भ में खुलकर विश्लेषण पहली बार हुआ है और इसके लिए लेखक द्वय बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये बात सामने आयी है कि कैसे एनएचआरसी ने कह दिया कि ईसाइयों के विरुद्ध हिंसा पूर्वनियोजित नहीं थी, जबकि उसके पास इसके पूरे तथ्य थे. इसी प्रकार पुलिस को क्लीन-चिट देना कि उनका दंगाईयों के साथ कोई लेना-देना नहीं था, जबकि उन्हीं की रिपोर्ट यह कहती है कि फुलबनी, रायगढ़ और पदमपुर में पुलिस की उपस्थिति में ही हिंसा हुई और पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, जिससे अपराधियो के हौसले बुलंद हो गए.
हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किन परिस्थितयों में हुई और इसकी क्या सीमायें हैं. मैं यह बात यहां रखना चाहता हूं कि भारत में अधिकांश आयोगों में उन लोगों की नियुक्तियां होती हैं, जिनका उन विषयों पर काम का न तो कोई अनुभव रहा है और न ही इस सन्दर्भ में उनका कोई इतिहास. ज्यादातर नियुक्तियां राजनैतिक होती हैं, जो लालबत्तियों की खातिर होती हैं. हालांकि गुजरात के दंगो के सिलसिले में मानवाधिकार आयोग ने कुछ अच्छा कार्य किया. इसमें कोई दो राय नहीं कि इन आयोगों में एक भी शब्द आने से लोगों में विश्वास जगता है, लेकिन आयोग की भूमिका उन मसलों में ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, जो मामले राजनैतिक दिखते हैं और जहा शक की सुई सत्ताधारी पक्ष पर जाती हो. आयोग उत्तर पूर्व और कश्मीर के मसले पर भी बहुत कुछ नहीं कर पाया है और न ही भारत में जातीय और धर्म आधारित भेदभाव के ऊपर ज्यादा प्रभाशाली बात रखने में सक्षम हुआ है.
पुस्तक के तीसरे अध्याय में पूरी न्यायिक प्रक्रिया का बहुत विस्तारपूर्वक विश्लेषण है, जो साम्प्रदायिकता के प्रश्नों और राजनीती से प्रेरित सामूहिक हिंसा के सवालों पर काम करने वाले लोगों और विशेषज्ञों के लिए अत्यन्त आवश्यक है. ऐसा इसलिए भी ज़रुरी है क्योंकि हिंसा के बाद किसी भी स्थान को एक तीर्थस्थल में तब्दील कर देना हमारे हवाई कार्यकर्ताओं और मीडिया का ‘नैतिक” कार्य बन चूका है. लेकिन घटना को लंबे समय तक फॉलोअप करने ले लिए बहुत धैर्य, संघर्ष और सैद्धान्तिक निष्ठा की ज़रुरत होती है. हमने जो अधिकांश ऐसे मामले देखे हैं, वहां पर क़ानूनी परमर्शदाताओं से लेकर ‘सामाजिक कार्यकर्त्ता’ अख़बारों में छपास टीवी पर दिखने की बीमारी से ग्रस्त नज़र आते हैं, लेकिन इस पुस्तक को देखने बाद लगता है कि यदि ईमानदारी के साथ तथ्यों को इकठ्ठा किया जाए और जनता के साथ लगातार संवाद की स्थिति हो तो लोगो को न्याय मिल सकता है.
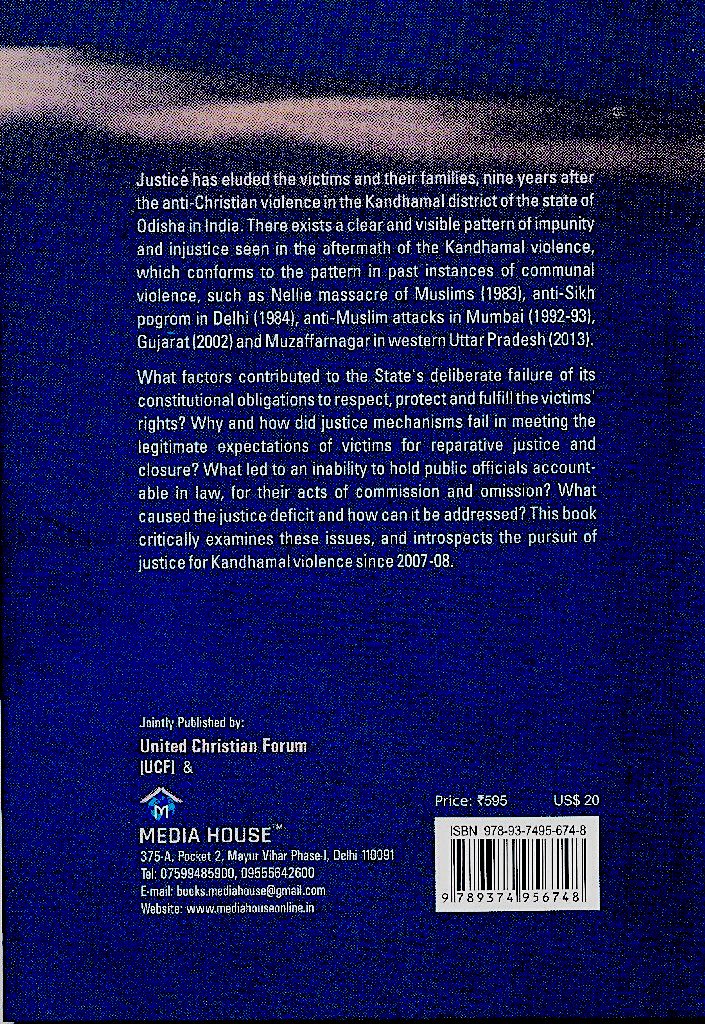
जब हम न्याय की बात करते हैं तो मात्र किसी को जेल पहुंचाना या सज़ा दिलवाना न्याय नहीं है, अपितु प्रभावित लोगों को मुआवजा, उनका सम्मानपूर्वक पुनर्वास न्याय प्रक्रिया का बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए, जो भारत के अधिकांश मामलो में नहीं हुआ है. क्योंकि मीडिया और पब्लिसिटी में ”फांसी का फंदा” ज्यादा टीआरपी वाला होता है, लिहाज़ा असली बातें छूट जाती हैं.
मुझे पता है कि कंधमाल के लोगों को न्याय दिलवाने के लिए मानवाधिकारों के लिए संघर्षरत साथी जॉन दयाल और फादर अजय कुमार सिंह ने बहुत भाग दौड़ की है और लगातार दस्तावेज़ों को इकठ्ठा करने और गवाहों के साथ मज़बूती से खड़े होने के लिए बहुत संघर्ष किया है और उसी का नतीजा है कि ये केस अभी लगातार चल रहा है और लोगो में विश्वास की भावना जगी है.
हम सभी जानते हैं कि दंगे होते नहीं हैं, प्रायोजित करवाये जाते हैं. और उन जगहों के ताक़तवर लोग उसके पीछे होते हैं जिन्हें भरोसा होता है कि उन्हें राजनैतिक प्रश्रय मिलेगा और ब्याज सहित राजनैतिक लाभांश भी मिलेगा.
1974 से लेकर, 2002 से 2012 गुजरात, फिर आम चुनाव और अब उत्तर प्रदेश साम्प्रदायिकता की फ़सल लगातार मज़बूत हो रही है और उसका कारण सेक्युलर ताक़तों की न केवल कमज़ोरी है अपितु क़ानून के लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय मापदंडो को पूर्णतः लागू करवाने में हमारी असफलता भी.
बहुत समय से हम कम्युनल वायलेंस बिल की बात कर रहे थे कि सामूहिक नरसंहार या हिंसा में मारे जाने पर आज तक देश में एक भी व्यक्ति को सज़ा नहीं हुई, क्योंकि न तो गवाह मिलते और न ही पुलिस और एजेंसियां जो जांच करती हैं, उन्हें इन बातों में बहुत दिलचस्पी होती है. बहुत सी बातें केवल क़ानूनों के बदलने या बदलने से ही नहीं होंगी अपितु हमारे नज़रिये को भी बदलना पड़ेगा.
एक जांच अधिकारी यदि जातिवाद या सांप्रदायिक मानसिकता से ग्रस्त है तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि वह जांच को सही दिशा में ले जाएगा. मास वायलेंस में आज तक गवाह नहीं मिले तो क्या इसका मतलब यह कि हिंसा हुई ही नहीं. हिंसा को जस्टिफाई करने के लिए अफ़वाहों को सच्चाई का जामा पहनाया जाता है और कारण गिनाये जाते हैं और इस प्रकार क़ानून पीछे और हमारी आपसी मान्यतायें और अफ़वाहे ही हक़ीक़त बन जाते हैं. मीडिया इन अफ़वाहों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.
कंधमाल की हिंसा के गवाह लोगों को तरह-तरह की धमकियां मिली जिसके लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सरकार को निर्देश भी दिए. कई लोगों को मौत की धमकी भी मिली और बहुतों को फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट के बाहर अपहृत कर लिया गया. कुछ गवाहों को उनके वकीलों के चैम्बर और घरों से अपहृत कर लिया गया. कोर्ट के अंदर भी अपराधियों और आरोपियों के समर्थकों की भीड़ रहती जो गवाहों को लगातार भयग्रस्त रखता. इन सभी का विस्तारपूर्वक ज़िक्र इस पुस्तक में है. गवाहों को चुप रहने के लिए दवाब के घटनाओं के बारे में भी इसमें जानकारी दी गयी है. मैं तो केवल ये कह सकता हूं कि देश की राजधानी के पटियाला हाउस कोर्ट में कन्हैया कुमार वाले घटनाक्रम को देखने के बाद तो साफ़ ज़ाहिर है कि हमारी न्याय प्रणाली और उसके लिए काम करने वाले लोगों पर किस प्रकार का संकट है और जो दिल्ली में हो सकता है तो कंधमाल और अन्य क़स्बों के न्यायालयो में किस प्रकार का माहौल होगा उसकी कल्पना की जा सकती है.
एक नई बात हो रही है. जो इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में है कि कैसे उत्पीड़ित लोगों को ही आरोपित बनाकर उन्हें झूटे मुक़दमो में फ़साने की कोशिश हो रही है. न्याय प्रक्रिया गरीब के साथ में दिखाई नहीं देती और अदालतों में वकीलो के चक्कर काटना उनके लिए उत्पीड़न की एक नई श्रृंखला है, जिससे बच पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ताक़तवर लोगों के पास न्याय को देर कर देने के अनेक साधन हो चुके हैं और गरीब कुछ समय के हरासमेंट से जंग हार जाता हैं. हर बार कोर्ट के चक्कर लगाने के लिए उसे बहुत मेहनत और पैसे की ज़रुरत होती है.
इस शोधपूर्ण कार्य के लिए वृंदा ग्रोवर और सौम्या उमा को बहुत शुभकामनायें, क्योंकी पूरी पुस्तक में न केवल ह्यूमन राइट्स लॉ के लिहाज़ से उनकी पकड़ नज़र आती है अपितु उनके विस्तृत कार्य और मानवाधिकारों के लिए उनकी निष्ठा भी दिखाई देती है. इसलिए ये पुस्तक मात्र एक अकैडमिक दस्तावेज़ ही नहीं है बल्कि लेखकों के मानवाधिकार के ज़मीनी संघर्षो के साथ जुड़े रहकर कार्य करने की विस्तृत समझ भी दर्शाती है.
ये पुस्तक बेहद आवश्यक है और उम्मीद करता हूं कि आज के दौर के सभी साथियों को न केवल जानकारी के तौर पर बल्कि नए विचारों के तौर पर भी भविष्य की रणनीतियों को निर्धारित करने के लिए काम आएगी. हम आशा करते हैं कि सभी राष्ट्रीय आयोगों के प्रमुख, सदस्य और क़ानूनविद भी इस पुस्तक को पढ़ेंगे और तदनुसार कार्यवाही करेंगे. सांप्रदायिक हिंसा की चुनौती से निपटने के लिए क़ानूनों और संबधित संस्थाओं की सीमाओ का जो विश्लेषण इस पुस्तक में है वो सभी के काम आएगा. मैं इस सन्दर्भ में केवल एक बात और जोडूंगा कि सांप्रदायिक या सामूहिक हिंसा विरोधी क़ानून बनाने का समय आ चुका है और इस पर कम से कम बहस तो शुरू हो जानी चाहिए.
पुस्तक काम नाम : Kandhamal : Introspection of Initiative for Justice 2007-2015 (कंधमाल : न्याय के लिए 2007-2015 तक किये गए प्रयासों का आत्मावलोकन)
लेखक : वृंदा ग्रोवर और सौम्या उमा
प्रकाशक : युनाइटेड क्रिश्चन फोरम व मीडिया हाउस
क़ीमत : 595 रूपये